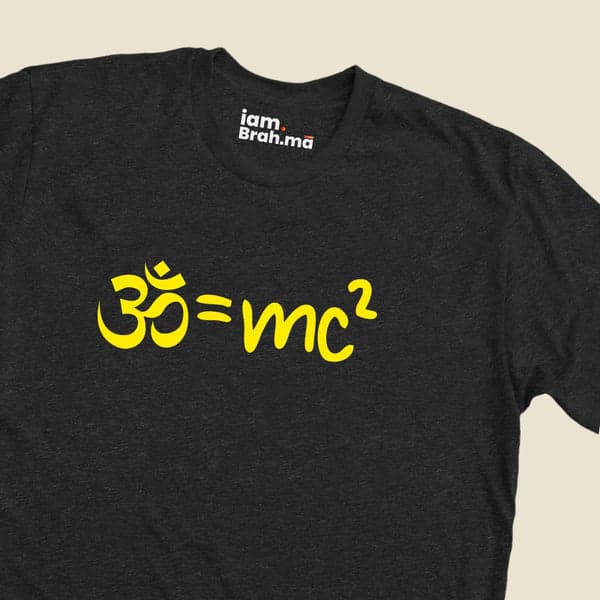बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रयास सभी करें !
परमात्मा की बनाई इस सृष्टि को कई अर्थों में अदृभुत एवं विलक्षण कहा जा सकता है । एक विशेषता इस सृष्टि की यह है कि यहाँ हर छोटे-से-छोटे घटक की अपनी एक विशिष्ट पहचान, अपनी एक मौलिकता है जो किसी दूसरे को उपलब्ध नहीं । एक चींटी, एक मक्खी के भीतर जो खासियत, जो विशेषता है- वो खासियत, वो विशेषता एक हाथी में या एक शेर में नहीं । यह ही तथ्य इससे विपरीत तर्क पर भी समानरूपेण लागू होता है । ऐसी ही एक विलक्षण मौलिकता मनुष्य के भीतर भी है, जो उसे अन्य प्राणियों से अलग करती एवं एक विशिष्टता प्रदान करती है ।
मनुष्य के भीतर यह विशिष्टता इस रूप में है कि मनुष्य एकही साथ सौभाग्य तथा दुर्भाग्य, दोनों ही संभावनाओं का चाहक है । हमारे जीवन में उपस्थित विभिन्न तरह की संभावनाएँ ही ये तय करती हैं कि मनुष्य अपने जीवन में सौभाग्य का चयन करेगा या दुर्भाग्य का । संभावनाएँ ही ये तय करती हैं कि हमारे जीवन में उत्कर्ष का पथ मिलेगा या पराभव का । संभावनाएँ ही ये तय करती हैं कि हम अपने जीवन में एक सुगंधित पुष्प की तरह खिल सकेंगे या फिर एक मुरझाए फूल की भांति गुमनामी के अँधेरों में विलीन हो जाएँगे ।
मनुष्य अकेला ऐसा प्राणी है, जिसके भीतर रावण बनने की संभावना है तो राम बनने का अवसर भी । मनुष्य के भीतर कंस बनने की संभावना है तो कृष्ण बनने का अवसर भी है । मनुष्य यदि अंगुलिमाल के रूप में एक दुर्दांत डाकू बनने की संभावना अपने भीतर रखता है तो भगवान बुद्ध के रूप में एक महापुरुष बनने का अवसर भी उसके पास है।
इसे आज की परिस्थितियों का एवं वातावरण का दुर्भाग्य ही माना जाना चाहिए कि आज इनसानियत को आतंकित करते अंगुलिमाल तो कदम-कदम पर मिल जाते हैं, परंतु वो करुणा की प्रतिमूर्ति बुद्ध कहीं नजर नहीं आते । जहाँ आसुरी प्रवृत्ति वाले नर-पिशाचों का जमघट-सा तो दिखाई पड़ता है, परंतु उन निशाचरों का नाश करके प्रकृति व समष्टि का कल्याण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखाई नहीं पड़ते ।
महापुरुषों एवं अवतारों जितनी ऊँचाइयों पर न भी जाएँ तो भी एक सामान्य व्यक्ति के स्तर पर वातावरण में व्याप्त अंधकार का जो प्रभाव दिखाई पड़ता है, उसे जानने के लिए किसी अतिरिक्त प्रमाण की क्या आवश्यकता है ?
यदि व्यक्ति पतन के मार्ग पर आगे चलना चाहे तो उसे अनेकों संभावनाएँ, सहयोगी, सुविधाएँ-सहजता से मिल जाती हैं, परंतु धर्म, न्याय, मानवता व उत्थान का पथ इतना एकाकी क्यों नजर आता है । समाज में व्यक्ति को भ्रमित करने व पतित करने के मार्ग तो अनगिनत दिखाई पड़ते हैं, परंतु उत्थान का पथ, उत्कर्ष का पथ, उन्नति का पथ ये बता पाने में समाज एकदम से अपने को अकेला पाता है ।
ऐसा लगता है कि समाज जिन आदर्शो पर स्थापित था, वो आदर्श ही कहीं लुप्त से हो गए हैं । मानवता के संरक्षण की बात तो दूर, लोग परिवार को बचाने के लिए भी प्रयत्न करते दिखाई नहीं पड़ते । दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी अपने देश में होने के वाबजूद हर व्यक्ति इतना अकेला, इतना एकाकी, इतना भ्रमित क्यों है ? हर इनसान अपने आप में अकेला, डूबा हुआ, विक्षुब्ध नजर आता है । जीवन का लक्ष्य, उत्देश्य कहीं खो से गए हैं ।
व्यक्ति बिखरे हुए हैं, परिवार टूटे हुए हैं एवं समाज अपने को नष्ट करने पर आमादा नजर आता है । ऐसा लगता है कि मानवता एक सामुहिक आत्महत्या के लिए तैयार-सी हो गई है । ऐसे में परिवर्त्तन की माँग समाज के हर कोने से उठती दिखाई पड़ती है।
एक बड़ा परिवर्तन समाज की शिक्षा-व्यवस्था भी माँगती है । इतने सारे कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के होते हुए भी आज के विद्यार्थियों का जीवन यदि ध्येयविहीन, मूल्यविहीन एवं उदृदेश्यविहींन नजर आता है तो लगता है कि किस तरह की शिक्षा हम दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं ?
जिस विद्यालय से विद्यार्थी को अनुशासन सीखना चाहिए था यदि वो अनुशासनहीनता सिखाने लगे, जिस विद्या के मंदिर से विद्यार्थी को नैतिकता का पाठ सीखना चाहिए था, यदि वो ही अनैतिकता का द्वार बन जाए और जिस शिक्षा-प्रणाली को समाज को जिम्मेदार नागरिक तैयार करके देने चाहिए थे, यदि वो शिक्षा-प्रणाली ही उदृदंड एवं उच्छिन्न नागरिक तैयार करके समाज को दे तो किसको दोष दिया जाए? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किस द्वार पर दुहाई लगाई जाए?
इस वर्तमान संकट के पीछे का एक प्रमुख कारण यह है कि समाज की दौड़ गलत दिशा में हो गई है । वैभव बढ़ाने व महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की अंधी दौड़ में हम व्यक्तित्व निर्मित करने के मूल उत्देश्य को ही भूल बैठे हैं शिक्षा का क्या इतना ही उदृदेश्य है कि वो एक पैसे कमाने वाले कर्मचारी तैयार करके समाज को दे दे, चाहे व्यक्तित्व की दृष्टि से वो पूर्णतया दिवालिया हों ।
यदि हम भारत के प्राचीन इतिहास को उठाकर देखें तो हम पाएँगे कि भारत में गुरुकुलों के, अध्यापकों के, विश्वविद्यालयों के केंद्र में सदा से ऐसे व्यक्तित्व रहा करते थे, जिनके स्वयं के जीवन में शिक्षाएँ प्रमाण के रूप में उपस्थित थीं । जब स्वयं का व्यक्तित्व ही दोषों की खदान हो तो ऐसे व्यक्तित्व कोमल मन को क्या शिक्षाएँ दे पाने की स्थिति में होंगे, पैसे का भंडार होना ही यदि शिक्षण संस्थानों को खोलने के पीछे का एकमात्र आधार रह जाए तो हम विद्यार्थियों को सोच क्या दे रहे हैं ?
इसके साथ ही हम यदि मानवता की वैज्ञानिक प्रगति का इतिहास उठाकर देखें तो यह स्पष्ट दिखेगा कि विगत ‘ दो-तीन सौ वर्ष इस दृष्टि से अभूतपूर्व रहे हैं । विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में एक विलक्षण पायदान हासिल करके हम लोग बैठे हैं । एक ओर हम चंद्रमा और मंगल पर जाकर बैठ गए हैं या उस तैयारी में हैं तो वहीं अपने स्वयं के मनों व अपनों से हम दूर-दूर नजर आते हैं ।
ऐसे सुख का क्या लाभ, जो हमारे मन की शांति क्रो हमसे छीन ले । आज तकनीकी की दृष्टि से इतने विकसित हम हो चले हैं, पर क्या उस तकनीकी का कुछ लाभ हमको मिल माता है वो परमाणु जो ऊर्जा पैदा कर सकता था, वो बम बनाता है । वो विज्ञान जो लोगों को खुशहाल कर सकता था, वो आतंकवाद के साधन बनाता है । वो तकनीकी जो घरों को आबाद कर सकती थी, वो युद्ध का तांडव रचती है ।
प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों ? ऐसा इसलिए कि जितनी मेहनत हमने इन यंत्रों को बनाने पर की, इन तकनीकों को विकसित करने में की, यदि उसी मेहनत का थोड़ा-भी हिस्सा हमने उस तकनीकी को चलाने वाले इनसान पर खरच किया होता, उसके व्यक्तित्व के परिमार्जन में लगाया होता तो शायद ये दिन देखने को न मिलते । साक्षरता मिल जाने से, डिग्री मिल जाने से व्यक्तित्व नहीं मिल जाते हैं । व्यक्तित्व के परिशोधन की जिम्मेदारी आज़ की शिक्षा-प्रणाली को अपने हाथों में लेनी होगी तभी कुछ सार्थक एवं सकारात्मक परिवर्तन हो पाना संभव है । अन्यथा मानवता के वीभत्स पतन को हम अपनी आँखों के सामने घटता हुआ देख रहे होंगे ।
ये बातें यहाँ लिखने के पीछे का मंतव्य इतना है कि यह सत्य है कि हम भारत भर के स्कूलों, कॉलेजों को नहीं बदल सकते, पर हम इसके समानांतर बाल संस्कारशाला की व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकते हैं ।
...